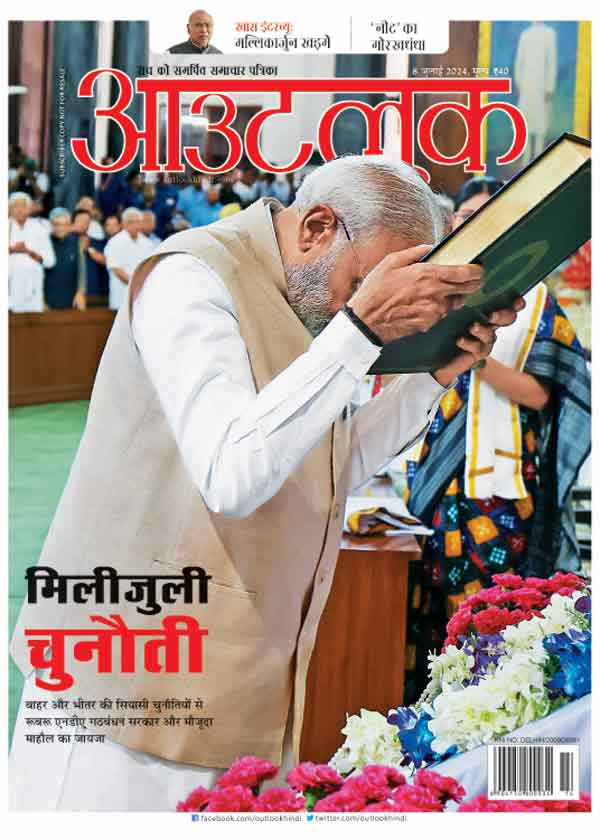लोकसभा चुनाव के परिणाम जो पंजाब से आए हैं, उनके सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इस सरहदी सूबे में स्याह ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं. हालांकि प्रदेश की कुल तेरह सीटों में से सात सीटें जीत कर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी एवं अकाली दल को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा की जीत उन्हें बेचैन करती है जिन्होंने हथियारबंद चरमपंथियों की गतिविधियों के कारण अपनों को खोया है. भारत को एक राष्ट्र के रूप में सफल नहीं रहने देने के लिए औपनिवेशिक शासकों ने न केवल मुस्लिम लीग के नेताओं को उकसाया था बल्कि अकाली नेताओं को भी पहचान आधारित राजनीति के लिए प्रेरित किया था.
बहुधर्मी एवं बहुभाषी देश भारत का संविधान सभी वर्ग के लोगों को राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक न्याय की गारंटी देता है. राष्ट्रवादी सिखों ने खालिस्तान की मांग से हमेशा खुद को अलग रखा. मुस्लिम लीग के नेताओं को अपने समुदाय के लिए पृथक् देश "पाकिस्तान" मिल गया. किंतु इस मजहबी मुल्क के बन जाने के बाद हुए रक्त-रंजित दंगों और शरणार्थियों की भीषण समस्या के कारण हिंदु-सिख एकता इतनी मजबूत हो गयी कि पृथकतावादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगने लगा. लेकिन स्वायत्तता की मांग ने माहौल को विषाक्त करना शुरू कर दिया.
गौरतलब है कि 1973 में पारित आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ने सिख जीवन पद्धति के प्रचार पर बल देते हुए एक "नए पंजाब" के गठन पर जोर दिया था. बाद के वर्षों में अकाली दल के नेताओं ने चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने हेतु "आनंदपुर साहिब प्रस्ताव" को क्रियान्वित कराने के लिए आंदोलन करने लगे जिसके परिणामस्वरूप पंजाब अशांत हो गया. संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में कट्टरपंथियों की एक नई जमात खड़ी हो गयी. स्वायत्तता की मांग तब अर्थहीन प्रतीत होने लगी जब सिख पुनरुत्थानवाद की धारा प्रवाहित होने लगी थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फरवरी 1983 में समाधान की दिशा में कदम उठाते हुए अकालियों की धार्मिक मांगों को स्वीकार करने की घोषणा की. लेकिन धर्म और राजनीति को मिश्रित करने की कोशिशें अलगाववाद के पैरोकारों के हौसले बुलंद कर रही थीं.
1980 के दशक में खालिस्तान की मांग को शहरों एवं कस्बों तक पहुंचाने में अंग्रेजी पढ़े-लिखे एवं कुर्सी-लोभी लोगों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता. अकाली दल के नेता तो राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल रहे, किंतु जगजीत सिंह एवं उसके सहयोगी "पृथक् सिख राज्य" की स्थापना के लिए बेचैन थे. पंजाब में आतंक फैलाने के लिए गैर-सिखों पर हमले होने लगे. स्वर्ण मंदिर में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के कारण स्थिति बद-से-बदतर होती गयी. अंततः ऑपरेशन ब्लू स्टार का निर्णय लिया गया. यद्यपि इस सैन्य कार्रवाई की काफी आलोचना हुई तथापि इसने राष्ट्र रक्षार्थ केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा-शक्ति को मूर्त रूप देने का काम किया. सिख समुदाय के नेता ही नहीं बल्कि आम जन भी इंदिरा गांधी के इस फैसले से असहमत थे. 1984 के अक्टूबर महीने की आखिरी तारीख को देश में उस वक्त शोक की लहर फैल गयी जब इंदिराजी के निधन की खबर प्रसारित की गयी. यह ऐतिहासिक तथ्य है कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षाकर्मियों ने ही की थी. अविश्वास के अंधियारे में उम्मीद की रोशनी दिखी राजीव-लोंगोंवाल समझौते में. अकाली नेता संत हरचंद सिंह लोंगोंवाल और युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मध्य हुए समझौते ने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की.
बीबीसी संवाददाता मार्क टली एवं सतीश जेकब ने अपनी किताब "अमृतसर : इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई" में राजीव गांधी के शांति प्रयासों की सराहना की है. लेखक द्वैय के अनुसार "पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए राजीव गांधी के फैसले से लगा कि उन्हें अहसास हो गया था कि साम्प्रदायिक कलह का जवाब पुलिस और सेना नहीं है. उन्हें लगा कि पंजाब की तात्कालिक समस्या को सुलझाने के लिए एक राजनीतिक साहस की जरूरत है. अगर उन्हें इस समस्या के असल कारणों से निपटना है तो उन्हें एक नयी तरह के संकल्प और साहस की जरूरत होगी और इसके लिए उन्हें भारतीय जीवन और सोच के हर पहलू को आधुनिक करने के रास्ते तलाशने होंगे, देश को कोई क्षति पहुंचाए बिना उन्हें दोबारा कांग्रेस की रचना करनी पड़ेगी जिससे कि यह वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पार्टी बन सके, लेकिन इस बार आधुनिक सामाजिक और आर्थिक नीतियों के साथ, उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का खून चूसने वाले परोपजीवियों - राजनीतिज्ञ, नौकरशाह और ठेकेदारों का शिकंजा तोड़ना होगा."
कई वर्षों तक पंजाब ने राष्ट्रपति शासन का दौर ही देखा. इसके बावजूद पंजाबवासियों का राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास डिगा नहीं. 1990 के दशक के शुरूआती वर्षों में ही राज्य में चुनावी राजनीति कामयाब होने लगी. कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा एवं वामपंथी पार्टियों की सक्रियता ने "खाड़कूओं" के प्रभाव को समाप्त कर दिया. के पी गिल की रणनीति से पंजाब पुलिस की को अपार सफलता मिली. हालांकि अमन बहाली के इसी दौर में प्रदेश ने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी खोया. लेकिन इससे लोकतांत्रिक शक्तियां कमजोर नहीं हुईं. सत्ता में आने का मौका अकाली दल और कांग्रेस दोनों को मिलता रहा. दहशतगर्दी की गर्म हवाओं का बहना थम-सा गया था. लेकिन उत्तर अमेरिकी देश कनाडा, पंजाब की खुशियों को तबाह करने के लिए तत्पर अलगाववादियों को पनाह दे रहा है. यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो लोकतांत्रिक कनाडा के लिए मुसीबत लेकर आ सकती है.
जब केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून बनाए थे तो असंतुष्ट किसानों के विरोध-प्रदर्शन की प्रकृति को संतुलित नहीं माना गया था और ऐसी खबरें आने लगीं थीं कि खालिस्तानी तत्व हालात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं. इन दिनों पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं जिनकी प्रशासनिक क्षमता उम्मीद नहीं जगा पाती है. अकाली दल को अपनी चुनावी हार की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के आर्थिक विकास में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. अकाली नेत्री हरसिमरत कौर तो भटिंडा से जीत दर्ज करने में सफल हुईं लेकिन संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारामूला से अलगाववादी विचारधारा के समर्थक शेख राशिद की जीत और नेशनल कांफ्रेंस के दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला की हार यह बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा बलों के समक्ष चुनौतियां कम नहीं हुई हैं.
(लेखक प्रशान्त कुमार मिश्र स्वतंत्र पत्रकार हैं।)